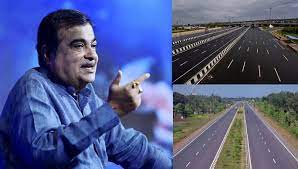औरत को कष्टों से उभारने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है कि उसे मूलभूत अधिकार दिए जाएँ।
संत्रति के विकास में सहायक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता मनुष्य महत्वाकांक्षा, हर्ष, विषाद, रचनात्मकता जैसे अभिलक्षणों के साथ नैतिकता,मानवता, सौहार्द आदि गुणों को प्रकट करते हुए ना केवल समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। बल्कि वह कल्याणकारी राज्य हेतु अपनी विशिष्टता प्रकट करते हुए, प्रकृति की रक्षा करता है। विभिन्न त्योहारों, मेलौ,एवं मनोरंजन आदि के अन्य क्रियाकलापों में कानून को अपने साथ दर्शाता है। यद्यपि स्वभाव से स्वार्थी यह सामाजिक प्राणी सुंदर, सम्मानजनक एवं स्थाई भविष्य की कामना रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने का प्रयत्न करता है। मानव जीवन के विभिन्न पृष्ठों को अगर बारीकी से देखा और परखा जाये तो दो महत्त्वपूर्ण पहलू उभर कर आते हैं।पहला यह कि प्रकृति और मनुष्य दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता अनन्त काल तक है, आज का वैज्ञानिक युग भी इस कथन को नहीं नकार सकता। दूसरा पहलू यह कि औरत और आदमी दोनों एक दूसरे की पूर्णता का आधार है और पहले पहलू की पूर्ण व्याख्या के लिए दूसरे पहलू को मजबूत करना आवश्यकता है।
जॉन मूर, रशेल कार्सन, एङवर्ङ ऐबै,हसदेवाचार्य जैसे आदि व्यक्तित्वौ ने बहुत पहले ही हमें यह दिखाने की कोशिश की,कि प्रकृति हमसे है बिलकुल वैसे ही जैसे हम प्रकृति से हैं यदि हम प्रकृति को खनन, प्रदूषण आदि के माध्यम से ठेस पहुंचाते हैं तो प्रकृति स्वयं को संतुलित करने का प्रयास करती है फलतः भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट,अनियमित मानसून,सूखा मानव जाति को अपना ग्रास बनाते हैं और कभी-कभी यह असाधारण रूप में सभ्यताओं को भी नष्ट कर देते है य।द्यपि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों की मानव द्वारा हनन करने के बाद प्रत्यक्ष विभीषिका है।परंतु प्रकृति द्वारा मानव जाति को दिए समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों की अनदेखी का मूल्य शायद ही इस सभ्यता को ज्ञात हो। प्रकृति स्वयं यह सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण वैश्विक समाज में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे बनाए रखना है शायद इसीलिए ना पुत्र को पुष्प बनाती है ना पुत्री को प्रवाह। ना किसी को श्रेष्ठ और ना ही किसी को सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि कतरा कतरा अमूल्य धरोहर है।
पुष्प की सुगंध भी आवश्यक है और नदी के जल के प्रवाह का रुकना भी उचित नहीं है परंतु इस भूलोक के अधिकतर समाजों ने इन अधिकारों की व्याख्या अपने-अपने हितों के अनुरूप कर रखी है। इनमें से अधिकांश पुरुष जाति द्वारा शासित हैं और इनमें भी कुछ ऐसी यथास्थिति (प्राचीन समयानुसार)में है तथा कुछ वर्तमान के अनुसार बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय समाज भी इसी का विस्तृत भाग है।यद्यपि भारतीय सभ्यता व्यापक समय को समेटे हुए है फिर भी नारी अधिकारों की दृष्टि से पिछले लगभग 3500 वर्षों के इतिहास को ही गौर से देखा जाए तो यह छवि कभी अत्यंत गहरी एवं कभी अत्यन्त धुंधली नजर आती है।

हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए वक्तव्य “लड़कियों को हर हाल में पैतृक संपत्ति में हक मिलना चाहिए।” भारतीय समाज की शंकाओं को तोड़ने की ओर इशारा करता है वही शंकाएं जो समानता के अधिकार को धरातल पर नहीं लाने देना चाहती,जो संवैधानिक अधिकारों को पूर्णता देने की बजाय आधे-अधूरे एवं संकुचित विचारों को जन्म दे रहीं हैं।यही शंकाएं औरत की वेदना को समझने की बजाय,उसका उपाय निर्मित करने की बजाय उसके दर्द से खेलती हैं। कठिन होता है इस सत्य को आत्मार्पित करना कि यह वही भारतीय समाज है जहाँ कभी सिंधु की मात्रसत्ताएं खेलती थीजहाँ विसफला जैसी योद्धा,घोसा,अपाला,सिकता एवं लोपामुद्रा के साथ अपने अमाजू धर्म (आजीवन कुँवारी रहकर शिक्षा ग्रहण)स्वीकार करने की बात करते थीं (संभवत)।उत्तर वैदिक तक आते-आते प्रधानमंत्री पद पर आसीन जनकसुता ‘सीता’ के दरबार में गार्गी अपने प्रश्नों के उत्तर याज्ञवल्क्य से मांगती नजर आती थी दूसरी ओर अथर्ववेद में ‘पुत्री जन्म को दुख का कारण’ बताने वाले कथन को झूठ साबित करने की कोशिश में मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट अशोक अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म का दायित्व सौंपता था। ताकि समस्त आर्यावर्त में पुत्रियों के प्रति आचरण को नयी एवं अविस्मरणीय दिशा मिल सके और आने वाली पीढ़ियां औरत जाती को मात्र देवी की संज्ञा देकर ना छोड़ दे, बल्कि अपने व्यवहार,विचार आदि में औरत को समान जीवन जीने का हक दे,इसी परम्परा के प्रवाह को अविचलित ना करते हुए सल्तनत काल में इलतुतमिस साम्राज्य की बागडोर अपनी पुत्री रजिया को देता है।
इतिहास ऐसे हजारों उदाहरणों से अटा पड़ा है जिसमें महिलाएं साम्राज्ञी भी रहीं हैं साथ ही ऐसे कई उदाहरण हैं कि वे किंग में कर भी रही हैं। महाम अनगा, मेरु निशा इसका अच्छा ही नहीं वरन निकट उदाहरण भी है, बावजूद इसके कि इतिहास में पुत्री ने अपने धर्म का निर्वहन भली-भांति किया उन्हें उनके ना जाने कितने ही अधिकारों से वंचित रखा गया। फलस्वरुप “बेटी सिर्फ एक बेटी ही बनी रही, बेटी होना क्या होता है यह कभी नहीं जान ही नहीं पायी।” इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, मातृभूमि का अधिकार। जो बेटे की भाँति बेटी के लिए भी नींव का कार्य करता। परंतु यहां भी एक बेटी को ही वंचित रखा गया।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों से राज्य लिंग, जाति,धर्म, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है15(1)।बोलने की स्वतंत्रता,जीवन की सुरक्षा,कानून के समक्ष समान संरक्षण जैसे आदि अधिकार प्रदान करता है एवं इनकी अनिवार्यता भी सुनिश्चित करता है क्योंकि भारतीय समाज स्वयं के अस्तित्व को प्राचीन परंपराओं,मान्यताओं,धार्मिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखता है। परन्तु इस प्रक्रिया में समय के साथ (विभिन्न काल खंडों में,विभिन्न प्रयोगों द्वारा)विभिन्न जाती विशेष के धर्माचार्यों द्वारा धर्म शास्त्रों की गलत व्याख्या करके सामाजिक एवं रुढ़िवादी तत्व जोड़ दिए गए या कहें कि पुरुषों ने,पुरोहितों ने, पुरुष श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अर्थात् स्थापित करने के लिए विभिन्न मान्यताओं को स्वयं विवेक से जोड़ दिया जिसे तोड़ने या सीमित करने का प्रयास यदि किया जाए तो मान्यता की क्षति को भी साथ लिख दिया गया। सीधे शब्दों में यदि कहें तो कुरीतियों को सीमित करने से भी रोक दिया गया।
इन रुढियों, अंधविश्वासों, और स्त्री अधिकारों के विपरीत जन्मी मान्यताओं से भय खाए समाज का पुरुष वर्ग ही नहीं वरन महिलाएं भी इन्हें झुठलाने में खुद को असहज पाती है।स्वयं के अधिकारों को मांगना तो दूर स्वयं पर दुराचार के प्रश्न भी नहीं उठाती है यही कारण है, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन के फल स्वरुप 2005 में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में क्लास एक कानूनी वारिस के रूप में हिस्सा देने के उपरांत भी यह अधिकार पुरानी फाइलों की तरह धूल फांक रहा है।’स्टेट ऑफ लेंड रिपोर्ट 2018′ के अनुसार, मात्र 12.9% महिलाएँ अपनी इस भूमि के अधिकार का उपयोग कर पाती हैं।
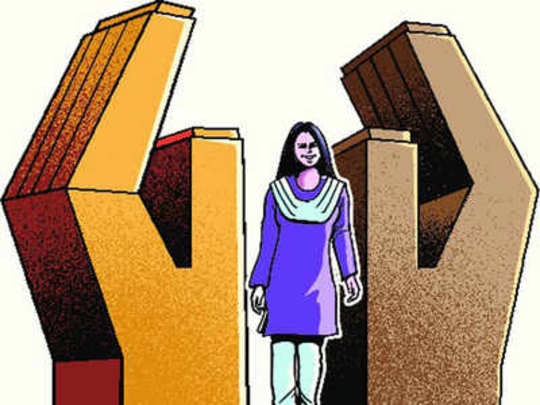
सन 1951 में, जिस देश का लिंगानुपात 946, साक्षरता दर 18.33% से परिवर्तित हो कर क्रमशः 943 एवं 74.04 प्रतिशत हो गयी हो।अर्थात निरंतर सफलताओं के उपमान रचे जा रहे हो, वहॉं नारी के पैतृक संपत्ति में अधिकार के प्रति समाज की ये उदासीनता उचित नहीं। 21वीं सदी के 21वे वर्ष में होने के बाबजूद,हमारा समाज प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी सोच से भयभीत एवं कुंठित विचारधारा से शोषित हो रहा है।आधुनिक वैज्ञानिक युग में पुत्र द्वारा अंतिम संस्कार को स्वर्ग की सीढ़ी मानना (एवं इसी संदर्भ में पुत्र की नाराजगी से बचने हेतु पुत्री को समान अधिकार ना देना), सम्पत्ति का बँटवारा करने पर वृद्धआश्रम का भय रखना,बेटी के ससुराल की छाया तक को ऋण मानना, रिश्तों के टूटने का भय सताना,समाज के सम्मानीय नजरिया में कमी का एहसास करना एवं चार आदमी क्या कहेंगे वाले ध्येय वाक्य को प्रति क्षण हृदय में अवस्थित रखना इत्यादि पूर्वाग्रह हमें ना केवल प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करने को बाध्य कर रहे हैं अपितु संपूर्ण विश्व के परिपेक्ष्य में स्वयं को पिछड़ा साबित भी कर रहे हैं। उपरोक्त भय को शांत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा कही गई एक पंक्ति ही काफी है,”बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं,जबकि बेटे बहुओं के आने तक ही बेटे रहते हैं”।कथन आत्मीयता लिए हुए हैं, इसलिए आत्मसात करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देना ना केवल रूढ़िवादी सोच को हमारी परंपराओं से हो उपाटेगा,बल्कि यह दहेज,घरेलू हिंसा,पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ आदि संकुचित मनोवृत्ति से निजात पाने का सुद्र सुदृढ़ आधार भी साबित होगा एवं भारतीय समाज में ना केवल खोखली मानसिकताएँ टूटेंगी,ना केवल महिला सशक्तिकरण को नयी दिशा मिलेगी, वरन् एक बेटी को यह एहसास भी होगा कि वह अब पराई नहीं है, एवं सम्पत्ति का हक होने से निःसंदेह आत्मसम्मान का भाव विकसित होगा जिससे सम्भव है कि घरेलू हिंसा का जवाब भी प्रत्यक्ष रूप में दिया जा सकेगा।पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को अनिवार्य करके अवश्य ही बेटी के भग्नमनोरथ पूर्ण किया जा सकते हैं। इससे आत्मविश्वास की व्याख्या भी सीमित नहीं रहेगी।सम्भवतः स्थाई संपत्ति भाई से संबंधों को तोड़ने की बजाय बचपन को संजोने का जरिया बन जाए।
अहिंसा के पुजारी गांधीजी की धरती पर एवं आर्यों द्वारा रचित वेदो के दर्शन के अंतर्गत जहाँ ‘देने’ का सुख सर्वश्रेष्ठ हो, हमें इस ‘देने’ के भाव को संकुचित रूप में ना लेकर व्यापक अर्थों में ग्रहण करना चाहिए। ताकि फिर किसी स्त्री को अपने अधिकारों से वंचित ना रहना पड़े। जिस प्रकार कुशल राजनीतिज्ञ होने के बावजूद राजा सुभमति ने अपनी पुत्री कैकई को राजपाठ ना देकर अपने पुत्र को संपूर्ण साम्राज्य सौंप दिया,और कैकयी को इस दुःख की पीड़ा आजीवन भोगनी पड़ी एवं उसने अपने दुःख निवारण हेतु भरत को चुनना पड़ा(जैसा कि हमें हमारी लोक कथाओं में सुनने को मिलता है)। अर्थात् अब समय की महती आवश्यकता है कि जिस इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड कर तत्कालिक समाज अपने अनुकूल बनाया था उसे इन प्रतिकूल परिस्थितियों में सकारात्मक सोच के साथ दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां प्रश्न करेंगी और शायद इसका माकूल जवाब भी हम ना दे पायें, यह मात्र एक बेटी की ही नहीं संपूर्ण विश्व की मांग है, वक्त है उस इंसान से कुछ आशाओं को पूरा करवाने का जिसका एक पुत्री के जीवन पर, उसके मूल्यों पर एवं उसके चरित्र पर सर्वाधिक प्रभाव होता है यानी कि माता पिता।
परिवार,दुनिया के प्रत्येक प्राणी के जीवन की मूलभूत इकाई होता है।यह ना केवल श्रेष्ठतम विचारों, कार्यों,त्याग आदि की व्याख्या करता है अपितु सत्य,प्रेम, समर्पण, तथा विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों को संजोने के मायने भी बताता है।21वीं सदी का तीसरा दशक अपना डेरा डाल चुका है, मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाकलापों से जन्मी महामारी covid-19 ने विश्व को नयाचार करने के लिए प्रेरित नहीं बल्कि मजबूर किया है। पुनः वैदिक अवधारणा को व्यक्त करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है जानकी को दोहराने की, अपाला ,घोसा को जीवित करने की।ऋत की अवधारणा को निरंतर नकारने के कारण समाज अपने पतन की ओर जाने लगता है।व्यक्ति का समाज के प्रति और समाज का व्यक्ति के प्रति आचरण सब कुछ ऋत से बंधा हैl जो कि प्राकृतिक व्यवस्था एवं संतुलन को इंगित करता है।
नैतिक व्यवस्था का निर्माण भी इसी ऋत से होता है,जिससे मानव मात्र का व्यवहार पूर्णता की ओर अग्रसर होता है।जिस ऋत के बंदी सूरज,चंदा, तारे सब है।उस ऋत को आत्मसात करने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।ऋत के अनुसार जो निरंकुश हो जाये उसे नकारने में ही भलाई है, इसीलिए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में महिला एवं पुरुष के संतुलन को स्थापित करने के लिए आदिवासी समाज से बेहतर अन्य विकल्प नहीं हो सकता, यहां महिला और पुरूष समानता के प्रत्यक्ष प्रमाण देखे जा सकते हैं।गोंड,कंजर जैसी जनजातियों ने पुरुष के वर्चस्व की सर्वश्रेष्ठता को शानदार तरीके से नकारा है।

कहने को इनकी प्राचीनता पर, इनकी रूढ़िवादिता पर, वैज्ञानिक युग को नकारने के व्यंग गढ़े जा सकते हैं कहा जा सकता है कि यह आधुनिकता से परिचित नहीं है।हाँ!हम सभी ने भी आधुनिकता के नए आयाम जरूर तय किए हैं परंतु ये सब स्त्री विरोधी साबित हो रहे हैं।परंतु आदिवासी समाज ने ऐसा कदापि स्वीकार नहीं किया, बल्कि इन्होंने समय,आधुनिकता और तो और विज्ञान को मस्तिष्क में रखकर एवं परंपराओं को हृदय में स्थान देकर हर बार मानव जाति को चेताया है कि लड़की हो या लड़का दोनों के अंदर दिल एक ही धड़कता है।और ये दिल समय के साथ सामंजस्य बिठाना नहीं जानता, यही कारण है कि बेटियाँ बाहर तो छोड़ो घर में भी घुटन महसूस करतीं हैं यही घुटन समय के साथ मौत(आत्महत्या) में बदल जाती है।
इसलिए हमें नए नियमों,कानूनों को आत्मसात करने में पीछे नहीं रहना चाहिए।”लड़की की तरह लड़की व्यवहार ना करें लड़के की तरह लड़का व्यवहार ना करें।” किसी महान व्यक्ति के मुख से निकली ये पंक्तियां वर्तमान और भविष्य में प्रवेश करने का सबसे सुंदर मार्ग प्रतीत होती हैं। टेस्ला के मालिक द्वारा एक महाविद्यालय के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कही गयी बातें जो उनके विनम्र निवेदन में लक्षित थीं, ” हमें अपने जीवन में उस वस्तु के आयाम अवश्य बदलने चाहिये जिसे हम उस रूप में देखना चाहते थे लेकिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण हम उसे उस रूप में देख नहीं पाये।”अर्थात् उस प्रत्येक वस्तु, स्थिति, सीमा जिसने हमें आहत किया है उसे हमें अगली पीढ़ी के लिए अवश्य परिवर्तित कर देना चाहिए।कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता समाज को परिवर्तित करने की नहीं बल्कि समाज की मानसिकता को सुव्यवस्थित करने की है।जिससे बेटी और बेटा में मात्र मात्रा(ए और आ ) का ही अन्तर बचे ।

भावना चौधरी उन्देरा(आगरा)